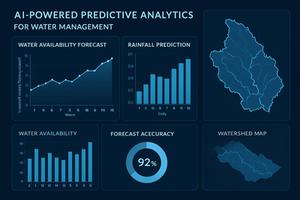पानी की कहानी - सिंधु नदी
- By
- Pani ki Kahani
- July-29-2019
संक्षिप्त परिचय -
एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लम्बी नदियों में शुमार सिंधु नदी संसार की प्राचीनतम नदियों में से एक है. इस नदी को ‘इंडस’ के नाम से भी जानते हैं. इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के समीप सिन-का-बाब नामक जलधारा को माना जाता है. लगभग 3200 किलोमीटर लम्बी यह नदी तीन देशों भारत, पाकिस्तान और चीन में बहती है. पाकिस्तान की सबसे लम्बी नदी होने के साथ- साथ सिंधु नदी वहां की राष्ट्रीय नदी भी है. शुरूआत में यह नदी तिब्बत से कश्मीर की ओर बहती है, जो कि आगे चलकर नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहते हुए अन्त में अरब सागर में जाकर समाहित हो जाती है.
ऐतिहासिक महत्व -
भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपनी गोद में पालन- पोषण करने वाली सिंधु नदी के तट पर ही कई ऋषि- मुनियों ने तपस्या की, तो यहीं पर कई वेद- पुराण भी रचे गए. इतिहास में इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के उत्तर में करीब पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर माना जाता है. सिंधु नदी के इतिहास में जब जातीय, धार्मिक और भाषागत विभिन्नताओं के चलते विभिन्न संस्कृतियां अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहीं थी, तब कई पारम्परिक भाषाओं जिनमें द्रविनियन, ईरानियन, पाली, प्रक्रित व संस्कृत शामिल हैं, ने मिलकर भारत की संस्कृति और सभ्यता को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया.
इतिहास के आधार पर सिंधु नदी हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानियों को अरब और ईरानियों से अलग करने वाली सीमांकन रेखा के रूप में जानी जाती है. जब अलेक्जेंडर अपने दल के साथ सिंधु नदी को पार कर भारत आया, तो उसने यह देखा कि यहां कि संस्कृति, भाषा, कपड़े, रहन- सहन, खान- पान आदि यूनान और ईरान देशों से बिल्कुल अलग है.
पौराणिक महत्व –
भारत व विश्व की प्राचीनतम नदियों में एक अहम स्थान रखने वाली सिंधु/ इंडस नदी का उल्लेख रामायण, महाभारत के साथ ही वेदों में भी मिलता है. खासकर ऋग्वेद में वर्णित 25 नदियों में से सिंधु नदी का सबसे महत्वपूर्व नदी के रूप में कई बार उल्लेख किया गया है. इस वेद में सिंधु व इसकी अन्य छह सहायक नदियों का संयुक्त रूप से ‘सप्तसिन्धवः’ नाम से उल्लेख है. जिसके अन्तर्गत सिंधु नदी व इसके वितस्ता, अस्किनी, परूष्णी, विपाशा, शतुद्री तथा सरस्वती नदी से मिलन का मार्मिक रूप से वर्णन किया गया है.
ऋग्वेद में सिंधु नदी के प्रवाह व इसकी सहायक नदियों से मिलन को उसकी वृषभ से तुलना करते हुए लिखा गया है, कि जिस प्रकार मेघों से पृथ्वी पर घोर निनाद के साथ वर्षा होती है, उसी प्रकार सिंधु दहाड़ते हुए वृषभ की तरह अपने चमकदार जल को उछालती हुई आगे चली जाती है.
इसके अलावा रामायण में सिंधु नदी का महानदी के रूप में, तो महाभारत में इसका सरस्वती और गंगा नदी के साथ उल्लेख किया गया है. विभिन्न वेदों और पुराणों में इस नदी का उल्लेख सिंधु नदी का भारतीय और हिंदू संस्कृति से संबंधित होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है.
सिंधु से पड़ा ‘हिन्दुस्तान’ का नाम –
सिंधु नदी के नाम के विषय में इतिहास में वर्णन मिलता है कि ईरान के लोग ‘स’ को ‘ह’ बोलते थे, जिस वजह से वो लोग सिंधु नदी के ‘हिंदू’ कहते थे. इसी काऱण सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को ‘हिंदू’ कहा जाने लगा. इसके बाद पारसी में सिंधु को ‘हिंदू’ कहकर संबोधित किया जाने लगा. जिसके आधार पर ही भारतवासियों को ‘हिंदू’ और भारतवर्ष को ‘हिंदुस्तान’ के नाम से जाना जाने लगा.
वहीं अगर इतिहास में सिंधु नदी के अन्य नामों की बात करें तो समृद्धि के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली इस नदी को इसके आर्थिक महत्व के कारण ‘हिरण्यनी’ कहा गया, तो वहीं इसके तट पर ऊन का व्यवसाय होने के कारण इसे ‘सुवासा’ नदी के नाम से भी जाना गया.
सिंधु का सफ़र –
तिब्बत की मानसरोवर झील के समीप से बहते हुए सिंधु नदी भारत की ओर मुड़ती है तथा जम्मू- कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करती है. भारत में प्रमुख रूप से लेह व हैदराबाद में प्रवाहित होने के बाद सिंधु नदी नंगा पर्वत से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की ओर बहने लगती है. यह नदी पाकिस्तान के बड़े भूभाग में प्रवाहित होती है तथा अंत में अरब सागर में मिलने के साथ ही सिंधु के सैकड़ों कि.मी. लम्बे सफ़र का अंत हो जाता है.
सहायक नदियां –
सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र अत्यन्त व्यापक व विस्तृत है, जिसके चलते इसके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशों की कई नदियां इसके मार्ग में नदी में आकर मिल जाती है. सिंधु नदी की यात्रा के दौरान बांयी दिशा से सिंधु नदी का झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सुरु जैसी प्रसिद्ध नदियों से संगम होता है. वहीं दाहिनी दिशा से इसमें गिलगिट, काबुल, कुनार, श्योक, स्वात आदि नदियां मिलती हैं. इसके अलावा कई छोटी- छोटी जल धाराएं भी इस दौरान सिंधु नदी में समाहित हो जाती हैं.
सिंधु जल संधि –
सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक ऐतिहासिक संधि हुई थी, जिसे सिंधु जल संधि के रूप में जानते हैं. जिसके अंतर्गत सिंधु नदी व इसकी पश्चिमी सहायक नदियों झेलम तथा चिनाब का पानी भारत द्वारा पाकिस्तान जाने से रोका नहीं जायेगा, जबकि पूर्वी सहायक नदियों ब्यास, रावी, सतलज के पानी का प्रयोग करने के लिए भारत पूर्णतः स्वतंत्र है. हालांकि भारत पश्चिमी नदियों के जल का भी कृषि व बिजली बनाने आदि कार्यों में सीमित उपयोग कर सकता है.
यह समझौता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू व पाकिस्तान के सैनिक शासक अयूब खान के बीच किया गया था, जिसकी विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी. भारत की राजनीति में सिंधु जल समझौता हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है तथा कुछ लोगों का मानना है कि इस संधि के चलते भारत को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है. इसके अलावा पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारतीयों द्वारा जब तब इस संधि को रद्द करने व सिंधु नदी का पानी रोकने की मांग उठायी जाती रही है. वहीं अगर भारत सरकार यह समझौता रद्द कर देती है, तो पानी की भीषण किल्लत के साथ ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है.